"शिक्षा प्रणाली में जीवन उपयोगी विषयों को अनिवार्य किया जाए": आचार्य रमेश सचदेवा
भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्र गणित,
विज्ञान और
भाषा जैसे विषयों में तो निपुण हो रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की
बुनियादी आवश्यकताओं से अनभिज्ञ रह जाते हैं।
आज के युवा पढ़ाई में तो कुशल हो सकते हैं,
लेकिन कर भरना
नहीं जानते, यातायात नियमों का पालन नहीं करते, मानसिक तनाव से जूझते हैं और आत्मरक्षा की तकनीक
से अनजान हैं। क्या यही हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था?
अब समय आ गया है कि सरकार, शिक्षा मंत्री
और नीति-निर्माता इस ओर ध्यान दें और छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न
रखकर, उन्हें जीवन के वास्तविक अनुभवों के लिए तैयार करें। इसके लिए जीवनोपयोगी
विषयों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना आवश्यक है।
आत्मनिर्भरता विकसित करने
वाले कौशल
आज के समय में आत्मनिर्भर बनना सबसे जरूरी है।
केवल पढ़ाई में अच्छे अंक लाकर जीवन में सफल नहीं हुआ जा सकता। एक व्यक्ति को अपने
छोटे-मोटे कार्य स्वयं करने आने चाहिए ताकि वह अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी
निभा सके। आत्मनिर्भरता केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
सफाई और स्वच्छता
स्वच्छता किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं
होती, बल्कि यह समाज के हर नागरिक का कर्तव्य होता है। भारत में सफाई की जिम्मेदारी
केवल सफाई कर्मचारियों पर छोड़ दी जाती है, जबकि जापान में हर छात्र को
अपने स्कूल, कक्षा और सार्वजनिक स्थानों की सफाई स्वयं करनी होती है। इससे उनमें अनुशासन,
स्वच्छता और
आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है।
विद्यालयों में छात्रों को स्वच्छता की
जिम्मेदारी दी जाए, जिससे वे न केवल अपने घर बल्कि समाज में भी सफाई बनाए रखने
में योगदान दें। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने की मानसिकता को समाप्त करने के
लिए छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
खाना बनाना और गृहकार्य
अधिकांश विद्यार्थी जब उच्च शिक्षा के लिए अपने
घर से दूर जाते हैं, तब उन्हें भोजन बनाने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह
केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम होता है।
विद्यालयों में यह सिखाया जाना चाहिए कि संतुलित
आहार क्या होता है, कैसे कम समय में पौष्टिक भोजन तैयार किया जाए, और किस प्रकार
बिना व्यर्थ खर्च किए भोजन प्रबंधन किया जाए। सप्ताह में कम से कम एक दिन छात्रों
को भोजन बनाने की व्यावहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
कपड़े धोना और प्रेस करना
आज के समय में बच्चों को अपने कपड़े धोना और सही
तरीके से प्रेस करना भी आना चाहिए। यह केवल व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ा नहीं है,
बल्कि अनुशासन
और आत्मनिर्भरता से भी संबंधित है। यह सीखना आवश्यक है कि कपड़ों की देखभाल कैसे
की जाए ताकि वे अधिक समय तक टिकाऊ रहें।
घर की मरम्मत और वाहन
देखभाल
छोटे-मोटे कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने
की मानसिकता को समाप्त करने की आवश्यकता है। विद्यालयों में छात्रों को यह सिखाया
जाना चाहिए कि यदि बिजली का कोई छोटा सा खराबी आ जाए, पाइपलाइन में कोई समस्या हो,
या फर्नीचर में
कुछ टूट जाए, तो वे स्वयं उसे कैसे सुधार सकते हैं।
इसके अलावा, वाहन की देखभाल के लिए भी
बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वाहन के
टायर बदलना, इंजन की देखभाल और ईंधन बचाने के उपाय कैसे किए जा सकते हैं।
सुरक्षा और आत्मरक्षा कौशल
आत्मरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं
है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा का भी हिस्सा है।
विद्यालयों में आत्मरक्षा को अनिवार्य किया जाना
चाहिए, विशेषकर लड़कियों के लिए। उन्हें कराटे, जूडो और मार्शल आर्ट्स जैसी
तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे किसी भी संकट की स्थिति में स्वयं
की रक्षा कर सकें।
इसके अलावा, आपातकालीन स्थितियों जैसे
आग, भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाओं और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपायों की जानकारी दी जानी
चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा और जीवन रक्षक तकनीकों को सिखाने
की व्यवस्था होनी चाहिए।
सामाजिक अनुशासन और
सार्वजनिक शिष्टाचार
सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन का पालन करना किसी
भी विकसित समाज की पहचान होती है। भारत में लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति
जागरूकता की कमी है, जिससे सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं।
विद्यालयों में यातायात नियमों की शिक्षा दी जाए
और यह सिखाया जाए कि सड़क पर पैदल चलते समय, साइकिल चलाते समय या वाहन
चलाते समय कौन-कौन से नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर
अनुशासन और शिष्टाचार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्यालयों में छात्रों को यह
सिखाया जाए कि लाइन में लगना, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना, महिलाओं का सम्मान करना,
और सार्वजनिक
संपत्ति की सुरक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है।
आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय
शिक्षा
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना भी उतना ही जरूरी
है जितना कि शारीरिक और मानसिक आत्मनिर्भरता।
विद्यालयों में कर प्रणाली, बैंकिंग
प्रणाली, बचत योजनाएँ, निवेश और बीमा की जानकारी दी जानी चाहिए। छात्रों को यह
सिखाया जाना चाहिए कि वे अपनी आय को कैसे प्रबंधित करें, व्यर्थ खर्चों से कैसे बचें,
और बचत की आदत
कैसे डालें।
हर कार्य विद्यालय करे यह
संभव नहीं, माता-पिता की भूमिका भी जरूरी
विद्यालयों में इन विषयों को लागू करना आवश्यक
है, लेकिन यह केवल विद्यालयों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। माता-पिता को भी इसमें भागीदारी
निभानी होगी।
यदि माता-पिता अपने बच्चों को घरेलू कार्यों में
हाथ बँटाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें
छोटी-छोटी जिम्मेदारियाँ दें, तो वे न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे
बढ़ सकते हैं।
यदि विद्यालय और माता-पिता दोनों मिलकर बच्चों
को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से भविष्य में वे अपने जीवन को
अधिक व्यवस्थित, अनुशासित और सफल बना सकेंगे।
सरकार और नीति-निर्माताओं
से अनुरोध
शिक्षा प्रणाली में इन विषयों को शामिल किया
जाना चाहिए ताकि हर विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सके। सरकार को चाहिए कि इन विषयों को
विद्यालयों में अनिवार्य करने के लिए उचित नीतियाँ बनाएँ और विद्यालयों में इन्हें
लागू करने की प्रक्रिया सरल करे।
यदि हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर और
जिम्मेदार नागरिकों का देश बने, तो हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन कौशल की शिक्षा
भी देनी होगी।
"शिक्षा वही, जो जीवन में
काम आए!"
रचनाकार : आचार्य रमेश
सचदेवा
निदेशक, ऐजू स्टेप फाउंडेशन
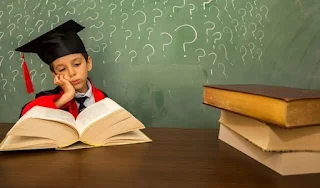
1 comment:
आज के समय की मांग💐👍
Post a Comment